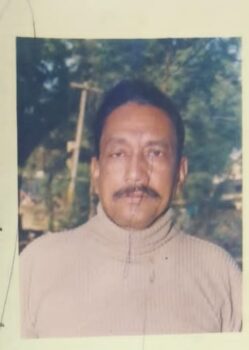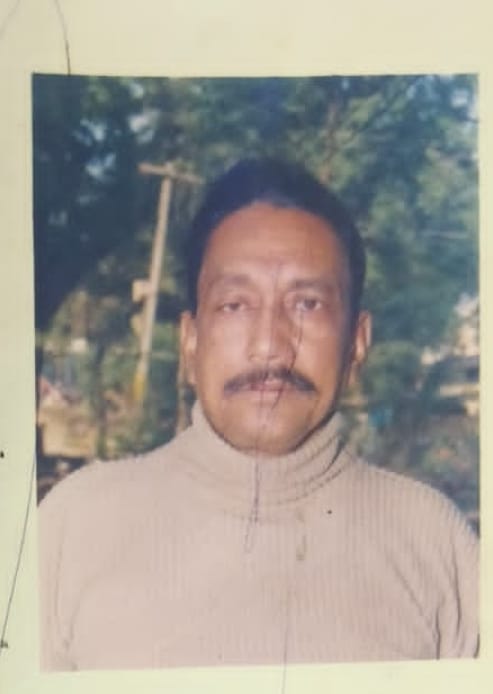✍🏽 लेखक – किरण रामी बाबूराव (मोहिते), नासिक, महाराष्ट्र
मो.नंबर 95618 83549
जब यह प्रश्न उठता है कि, “फूलें के असली दुश्मन कौन है?” तो आज भी अधिकांश लोगों के मन में एक ही उत्तर आता है – “ब्राह्मण समाज।” लेकिन यह उत्तर अर्धसत्य है। वास्तव में, ऐसे व्यापक निष्कर्ष निकालना भी उसी मानसिकता का प्रमाण है जो अज्ञानता, अंधविश्वास और भेदभाव से ग्रस्त है, जिसके खिलाफ महात्मा जोतिबा फुले ने अथक संघर्ष किया था।
फिल्म ‘फूले’ के रिलीज से पहले उसका ट्रेलर देखकर ही समाज में जो तूफान खड़ा हो गया है, वह सिर्फ ब्राह्मणों के प्रति नफरत के डर के कारण नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के इतिहास का सामना करने में असमर्थता को भी दर्शाता है। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म में ब्राह्मण समुदाय को बदनाम किया गया है, जबकि अन्य लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इतिहास का एक पक्ष चुना गया है। लेकिन यह प्रतिक्रिया केवल ब्राह्मण समुदाय की ओर से नहीं है; यह सम्पूर्ण भारतीय समाज का दर्पण है। क्योंकि किसी कार्य के पीछे के विचारों, अवधारणाओं और मूल्यों को समझने के बजाय, हम अभी भी पूछते हैं कि, वह कार्य किसने किया? वह कौन सी जाति थी? इस बात से अंदाजा लगाइये।
महात्मा ज्योतिबा फुले का आत्म-अनुभव इस मानसिकता के विकास का स्पष्ट प्रमाण है। अपने ब्राह्मण सहपाठी की बारात में भाग लेने मात्र से ही उन पर न केवल मौखिक बल्कि सामाजिक अपमान का सूखा और चुभने वाला कोड़ा बरसा, जिसने उनकी आत्मा पर गहरा आघात किया। उस घटना से उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे समाज में ‘शूद्र’ थे। और यहीं से एक ऐसी आग शुरू हुई जिसका उद्देश्य व्यक्तियों या समाज को क्रोधित करना नहीं था, बल्कि अन्याय की जड़ों पर प्रहार करना था। अगर उसने फैसला कर लिया होता तो वह आसानी से उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर अपने अपमान का बदला ले सकता था जिसने उसका अपमान किया था। हालाँकि, महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहचाना कि वह व्यक्ति या उसका समाज दुश्मन नहीं था, बल्कि उसके विचार ही उसके असली दुश्मन थे।
भारतीय समाज अभी भी व्यक्तियों को दोषी ठहराता है, समाज को दोषी ठहराता है, लेकिन उन दृष्टिकोणों को दोषी नहीं ठहराता।
नाथूराम गोडसे ने गांधीजी की हत्या की और जब यह पता चला कि नाथूराम गोडसे ब्राह्मण था, तो सभी जगहों पर पूरे ब्राह्मण समुदाय पर हमले शुरू हो गए। इनमें से नाथूराम गोडसे एक चितपावन ब्राह्मण था, जिसके कारण महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा हुई। पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, नागपुर और मुंबई सहित कई शहरों में ब्राह्मणों के घरों पर हमला किया गया, आगजनी की गई, लूटपाट की गई और उनकी हत्या की गई। उदाहरण के लिए, सतारा जिले में लगभग 300 गांवों में 1,000 से अधिक ब्राह्मणों के घर जला दिये गये। यह हिंसा न केवल गांधी की हत्या के प्रति आक्रोश से प्रेरित थी, बल्कि ब्राह्मण समुदाय के प्रति पहले से मौजूद घृणा और सामाजिक असंतोष से भी प्रेरित थी। यह हिंसा ब्राह्मणों के ऐतिहासिक प्रभुत्व के विरुद्ध आक्रोश को दर्शाती है, विशेष रूप से मराठा समुदाय के भीतर। इन घटनाओं के कारण कई ब्राह्मण परिवारों को अपना घर, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा खोनी पड़ी। उस समय मीडिया ने हिंसा की इन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए, इस घटना की विस्तृत जानकारी और दस्तावेज़ीकरण सीमित है। इन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने पर यह एहसास होता है कि किसी एक व्यक्ति के कार्यों के लिए पूरे समाज को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि नाथूराम गोडसे ने गांधीजी की हत्या करने से पहले पूरे ब्राह्मण समुदाय से परामर्श करके यह निर्णय नहीं लिया था। तो फिर एक व्यक्ति के गलत काम के लिए पूरे समाज को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? जब तक भारतीय समाज इस मुद्दे पर विचार नहीं करेगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और निर्दोष लोग मारे जाएंगे।
सिख नरसंहार 1984: निर्दोषों का खूनी इतिहास और भारतीय लोकतंत्र पर एक दाग
31 अक्टूबर, 1984. देश की दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से पूरा भारत हिल गया था। उनके अंगरक्षकों – सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जो सिख थे – द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर, पूरे देश में सिख समुदाय के खिलाफ बदले की भावना से प्रेरित हिंसा की लहर भड़क उठी। दिल्ली, कानपुर, भोपाल, इंदौर और देश के कई अन्य हिस्सों में हजारों लोगों को सिर्फ सिख होने के नाम पर मार दिया गया।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हिंसा में 2,732 लोग मारे गए, जिनमें से 2,146 अकेले दिल्ली में मारे गए। लेकिन मानवाधिकार संगठनों और स्वतंत्र रिपोर्टों का कहना है कि यह संख्या 8,000 से 17,000 तक हो सकती है। इनमें से अधिकांश मौतें सामान्य जीवन जीने वाले निर्दोष, निश्चिंत सिख नागरिकों की थीं।
कई शोध रिपोर्टों से पता चला है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई। कई गवाहों का कहना है कि दंगे योजनाबद्ध तरीके से किये गये थे। सिखों के घर जला दिए गए, उनके व्यवसाय नष्ट कर दिए गए, सिख महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार किए गए। लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुलिस और राजनीतिक मशीनरी पर इन सभी कृत्यों में निष्क्रिय या सहभागी होने का आरोप लगाया गया।
सवाल यह है कि क्या दो व्यक्तियों द्वारा किए गए क्रूर कृत्यों के लिए पूरा सिख समुदाय जिम्मेदार था? जवाब स्पष्ट है-नहीं. भारतीय संविधान के अनुसार, अपराध के लिए जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है, सामूहिक नहीं। लेकिन 1984 में इस बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। पूरे समुदाय की निंदा की गई तथा उनके अस्तित्व पर हमला किया गया।
कोई भी अपराधी या दुष्ट मानसिकता वाला व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने से पहले अपने पूरे समुदाय या धार्मिक अनुयायियों से परामर्श नहीं करता है। वह या कोई विशिष्ट समूह घटना को अंजाम देने के लिए सुनियोजित योजना बनाता है। उदाहरण के लिए, कश्मीर में हाल ही में घटित घटना, जिसमें आतंकवादियों ने कश्मीर में पर्यटकों से उनका धर्म पूछने के बाद उन्हें गोली मार दी, का उद्देश्य भारत में धार्मिक अशांति फैलाना तथा कश्मीरी लोगों के प्रति भारतीय समाज में असंतोष फैलाना था, जिससे पूरे देश में धार्मिक दंगे भड़क उठे। और कुछ जगहों पर, कुछ बहुत ही मूर्ख लोगों ने कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को निशाना बनाया और उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जहां तक भारतीय समाज का प्रश्न है, एक अपराधी का अपराध क्या है? और इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या है? जब तक यह बात समझ में नहीं आती, तब तक भारत में निर्दोष लोगों को जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता रहेगा।
महात्मा ज्योतिबा फुले किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति से द्वेष न रखते हुए उस सोचका विरोध करते थे,जो अमानविय हैं । उनमें परिवर्तन लाने के लिए वास्तव में क्या किया जाना चाहिए? इस बात को रेखांकित करते हुए उन्होंने स्कूल आंदोलन की शुरुआत की, तथा माना कि “अज्ञानता” ही मनुष्य का वास्तविक शत्रु है,तथा इस अज्ञानता को नष्ट करने के लिए मनुष्य का शिक्षित और सुशिक्षित होना आवश्यक है।
फुले की शैक्षिक क्रांति ब्राह्मण मित्रों के सहयोग से प्रज्वलित हुई थी – बौद्धिक मित्रता जिसने जाति की सीमाओं को तोड़ दिया था
भारत में बहुजनों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का पहला बड़ा प्रयास 19वीं सदी में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। महिलाओं, शूद्रों और अतिशूद्रों की शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया वह न केवल क्रांतिकारी था, बल्कि समाज को झकझोरने वाला भी था। लेकिन फुले इस यात्रा पर अकेले नहीं थे। उनके प्रयासों को कुछ प्रगतिशील ब्राह्मण मित्रों द्वारा दिया गया समर्थन अमूल्य साबित हुआ।
साल 1848. महात्मा फुले ने पुणे के भिडे वाडा में पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया. भिड़े ब्राह्मण समुदाय से थे। जबकि पूरी सामाजिक व्यवस्था महिला शिक्षा के खिलाफ थी, कुछ ब्राह्मण सहकर्मी फुले के पीछे मजबूती से खड़े थे। उन्होंने जाति प्रथा से नाता तोड़ लिया और सामाजिक परिवर्तन के लिए फुले के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया।
केशव सीताराम ढेरे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समुदाय के गुस्से की परवाह किये बिना, उन्होंने अपने घर में फुले के स्कूल के लिए जगह उपलब्ध करायी। उस समय एक ब्राह्मण द्वारा शूद्र-अतिशूद्र बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर खोलना एक साहसिक कदम था।
इसी तरह मराठी पत्रकारिता के जनक माने जाने वाले सदाशिव गोविंद जांभेकर ने फुले के विचारों को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। उनके लेखन में फूलों के काम की आवश्यकता और सामाजिक उपयोगिता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। शिक्षाविद् कोल्हटकर, अत्रे और भंडारकर जैसे विद्वानों ने भी इस सामाजिक क्रांति की विचार प्रक्रिया में योगदान दिया।
महात्मा फुले की वैचारिक परिपक्वता केवल उनकी अपनी जिद का परिणाम नहीं थी। उनके समान विचारधारा वाले मित्रों द्वारा प्रदान किया गया बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक समर्थन उनके आंदोलन के लिए शक्ति का स्रोत था। उन्होंने जाति की नहीं, बल्कि जाति-आधारित अन्याय की आलोचना की। इसलिए उन्होंने कभी भी सभी ब्राह्मणों को एकजुट विरोधी नहीं माना। उनकी मित्रता और सहयोग केवल सत्य के लिए था – सत्य को खोजने के लिए।
आज, जब हम सामाजिक समानता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, फुले और उनके ब्राह्मण मित्रों के बीच यह ऐतिहासिक साझेदारी प्रेरणा का स्रोत है। यहीं से हम सीख सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए न केवल उत्पीड़ितों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, बल्कि पूरे समाज की सचेतन शक्ति की भी भागीदारी आवश्यक होती है।
महात्मा फुले और तिलक: वैचारिक मतभेदों से परे राष्ट्रीय हित के आदर्श
महात्मा ज्योतिबा फुले और लोकमान्य तिलक दोनों महान विचारक थे जिन्होंने अपने-अपने तरीके से देश के लिए काम किया। यद्यपि उनके वैचारिक दृष्टिकोण विरोधाभासी थे – फुले सामाजिक सुधार, बहुजन शिक्षा और “ब्राह्मणवाद” के विरोध के समर्थक थे, जबकि तिलक राष्ट्रवाद, स्वराज और पारंपरिक हिंदू संस्कृति के समर्थक थे – फिर भी एक अवसर ऐसा आया जब फुले ने अपने मतभेदों को किनारे रखकर राष्ट्रीय हित के लिए तिलक की लड़ाई का समर्थन किया।
1897 में तिलक पर राजा रामकृष्ण अखबार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लेख लिखने के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तिलक को तब जेल में डाल दिया गया था और उनके लिए कोई गारंटर आगे नहीं आ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में महात्मा फुले आगे आये और बिना यह सोचे कि तिलक उनके विचारों के कट्टर विरोधी हैं और वे ब्राह्मण हैं, उन्होंने तिलक की मदद की।
यह घटना महज एक व्यक्तिगत या सांप्रदायिक असहमति है और वास्तव में ‘राष्ट्रीय हित सर्वोपरि’ के सिद्धांत का उदाहरण है। फुले ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि वैचारिक मतभेद व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो उसके साथ खड़ा होना हमारा सामाजिक कर्तव्य है।
यह ऐतिहासिक घटना हमें आज भी यह सिखाती है कि भले ही विचारधाराएं भिन्न हों, लेकिन देश के प्रति एक-दूसरे की सेवा को पहचानने और आवश्यकता पड़ने पर मदद का हाथ बढ़ाने की परिपक्वता अवश्य होनी चाहिए।
फूलें की करुणा और समानता का आदर्श: काशीबाई दीक्षित का मामला
महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले का जीवन न केवल शूद्र और अतिशूद्र समुदायों के उत्थान के लिए था, बल्कि सभी वंचित, पीड़ित और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए भी था – चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति का हो। इस महान मानवता का ज्वलंत उदाहरण एक ब्राह्मण विधवा काशीबाई दीक्षित के जीवन को बचाने और उसके बच्चे को गोद लेने की घटना है।
काशीबाई एक विधवा ब्राह्मण महिला थीं, जो अपने पति की मृत्यु के बाद समाज द्वारा अकेली, उपेक्षित और बेघर छोड़ दी गई थीं। उसने गर्भवती होने के दौरान ही आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। यह खबर सुनकर सावित्रीबाई फुले उसके घर पहुंचीं और उस महिला को ले आईं। उसे मनोवैज्ञानिक सहायता, घर और सुरक्षा दी गई।
बाद में काशीबाई ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया… “यशवंतराव फुले”. फुले ने उस बालक को गोद ले लिया और बड़े प्यार से उसका पालन-पोषण किया। यशवंतराव बाद में डॉक्टर बन गए और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे।
इस घटना से यह सिद्ध होता है कि महात्मा फुले और उनकी पत्नी ने कभी भी सांप्रदायिक द्वेष के आधार पर अपना कार्य नहीं किया। उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया – यानी जाति के आधार पर अन्यायपूर्ण वर्चस्व का; लेकिन एक ब्राह्मण महिला का समर्थन करना और उसके बच्चे को गोद लेना उस स्तर पर मानवता का सर्वोच्च आदर्श है।
शत्रु व्यक्ति नहीं, बल्कि विचार है!
— फूलें का संदेश समझिए, समाज का विभाजन नहीं, विवेक बढ़ाइए..!
हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘फुले’ ने कई लोगों के मन में एक नई बहस छेड़ दी है। यह भी सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने फिल्म देखने के बाद ब्राह्मण समुदाय के प्रति नकारात्मक भावनाएं व्यक्त कीं। हालाँकि, ये फिल्म के वास्तविक और मूल संदेश को समझे बिना निकाले गए मनमाने निष्कर्ष हैं।
‘फूलें’ सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का इतिहास है, मानवता के लिए संघर्ष है। महात्मा फुले का असली दुश्मन कोई व्यक्ति या कोई विशेष समाज नहीं था। उनके जीवन के तीन मुख्य शत्रु थे- अज्ञानता, अंधविश्वास और भेदभाव। इस तिकड़ी के विरुद्ध उनके पसंदीदा हथियार थे – शिक्षा, सत्य की खोज और समानता।
उन्होंने कभी भी जाति-आधारित घृणा को बढ़ावा नहीं दिया। इसके विपरीत, कई ब्राह्मण सहकर्मियों ने उनके कार्य में बहुमूल्य योगदान दिया। फुले, जिन्होंने एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई दीक्षित की जान बचाई और उसके जन्मे बच्चे को गोद लिया, ने दुनिया को मानवता का सर्वोच्च आदर्श दिखाया।
यदि फुले सचमुच किसी समाज से नफरत करते तो यह घटना नहीं होती।
इसलिए, यदि कोई भी फिल्म ‘फूलें’ देखने के बाद यह निष्कर्ष निकालता है कि “सम्पूर्ण ब्राह्मण समुदाय बुरा है”, तो यह विनम्र निवेदन है – यह फिल्म दोबारा देखें। फुले ने विवेक और करुणा का दीपक जलाये रखने का प्रयास किया। उन्होंने अपने आंदोलन में समाज के बुद्धिजीवियों को शामिल किया।
आज हमें असली दुश्मनों से लड़ना है – अंधकारमय विचारों से – न कि किसी विशेष समाज से। यदि हम व्यक्तियों या समाजों को दोष देते हैं, तो हम उनके संघर्ष के मूल को भी नहीं समझ पाते।
“आइये हम विचारों के खिलाफ युद्ध छेड़ें, व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। आइए हम फूलें के असली दुश्मन को समझें और उनकी शिक्षाओं के साथ न्याय करें। अन्यथा, हम ही उनके ऐतिहासिक बलिदान का अपमान करनेवाले होंगे।”